प्रिंट माध्यम और सृजनात्मक लेखन पर टिप्पणी लिखिये।Write a comment on print medium and creative writing.
Im not a robot
प्रिंट माध्यम और सृजनात्मक लेखन पर टिप्पणी लिखिये।Write a comment on print medium and creative writing.

पत्रकार का लेखन 'इति' के महत्त्व की अपेक्षा 'अर्थ' के महत्त्व पर केन्द्रित होता है। सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय', धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, राजेन्द्र अवस्थी, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, मनोहर श्याम जोशी, कन्हैयालाल नन्दन आदि ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने दोनों क्षेत्रों में सफलता और ख्याति अर्जित की। मनोहर श्याम जोशी, कमलेश्वर, मृणाल पाण्डेय, हिमाँशु जोशी जैसे लोगों ने प्रिण्ट मीडिया और इलैक्ट्रानिक- मीडिया दोनों में ही महत्त्वपूर्ण कार्य करके योगदान किया है।
यात्रा-वृत्तान्त- तीर्थ-यात्रा हो या पर्यटन की प्रवृत्ति यह विराट भू और जन दोनों से निकटता का अवसर देता है। प्राचीन काल में फाहियान और ह्वेनसांग, अलबरूनी जैसे लोगों ने अपने यात्रा-वृत्तान्तों को शब्दबद्ध किया। आज वे प्राचीन समय में देश और सभ्यता को जानने के महत्त्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो रहे हैं। प्रकृति के प्रति सहज आकर्षण ऐसे लेखकों- पत्रकारों के शब्दों को साहित्यिक गुणवत्ता देने के अतिरिक्त सौन्दर्य और ज्ञान की प्यास भी पूरी करता है। अज्ञेय (अरे यायावर रहेगा याद), राहुल सांकृत्यायन जहाँ साहसिकता और सौन्दर्यवृत्ति का परितोष करते हैं, वहीं निर्मल वर्मा का 'चीड़ों पर चाँदनी' और रांगेय राघव के यात्रा-वृत्तान्त, • अजित कुमार "सफरी झोले में" महत्त्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज कहे जा सकते हैं।
आज 'ग्लोब्लाजेशन' का युग है। हम दूसरे देशों और लोगों के बारें में जानना चाहते हैं-दूसरे के अनुभवों को बाँटना चाहते हैं। इसीलिए यात्रा-वृत्तान्त का लेखन और साहित्य में उसकी स्थापना हो रही है। यात्रा-वृत्तान्त आज साहित्य की स्वतन्त्र विधा के रूप में स्थापित हो गया है। बहुत से देशों की सरकारें पत्रकारों-साहित्यकारों को अपना देश देखने और उसके बारे में लिखने का मौका देती हैं। बहुत से लेखक अपने घुमुन्तू स्वभाव और खोजी प्रवृत्ति के कारण अपने खर्च पर पर्यटन कर अपने अनुभवों को लिखते हैं। यात्रा-वृतान्त सामान्य लेख नहीं। इसका लेखक पूरी आत्मीयता से दृश्य जगत को 'कहानी' के अन्दाज़ में कह सके, दार्शनिक रंग और पैनी दृष्टि से वर्णन कर सके तभी पाठक को तन्मयता दे सकता है।
साक्षात्कार (इण्टरव्यू)- साक्षात्कार या भेंटवार्ता आज की पत्रकारिता की महत्त्वपूर्ण जरूरत है। समाचार पाने का भी यह महत्त्वपूर्ण माध्यम है। सही साक्षात्कार एक कला है, जो अनजान या महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को जानने, उनसे किसी विषय, विधा या सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है- प्रामाणिक भी। किसी उत्सव, संगोष्ठी या समारोह के अतिरिक्त अप्रत्याशित घटने या आपात् स्थिति की जानकारी हासिल करने का स्रोत है।

साक्षात्कार लेते समय अपने विषय की पूर्व जानकारी हासिल करें। साक्षात्कार देने वाले को यह नहीं लगे. कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अपने प्रश्न सीधे और स्पष्ट रूप में करें। राजनीतिज्ञों के साक्षात्कार कई बार बड़े जटिल होते हैं। वे साफ़-साफ कुछ नहीं बताना चाहते। साक्षात्कारकर्त्ता को. प्रश्नों का ऐसा चक्रव्यूह रचना पड़ता है कि उससे सच्चाई निकलवा सके। पर यह सब हल्के-फुल्के आत्मीयता भरे सहज अन्दाज में किया जाय। ताकि साक्षात्कार .. देने वाला किसी डर या दबाव को अनुभव न करें। स्वयं अधिक न बोलकर साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को बोलने दें। आपके प्रश्नों में वह रुचि ले और अधिक से अधिक जानकारी दे। प्रश्नकर्ता को ऐसे प्रश्न संज़ोने चाहिए कि अधिक से अधिक जानकारी हासिल हो सके। कही गयी बातें उन्हीं के शब्दों में लिखें तो अच्छा रहता है। मिलते ही प्रश्नों की बौछार न करें। अनौपचारिक बातें करके भेंटकर्ता से आत्मीयता स्थापित करें। उसकी पुस्तकों अथवा कार्यों के विषय में जानकारी एकत्र करने के बाद ही साक्षात्कार उचित रहेगा। कलाकारों से साक्षात्कार के समय उनके भावी कार्यक्रम, प्रोजेक्ट के बारे में अवश्य पूछें। पिछले कार्यक्रमों की सफलता- असफलता या महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं और उनके महत्त्व पर भी बात कीजिए।
साक्षात्कार के लिए पूछे गये प्रश्न महत्त्वपूर्ण होने चाहिए। इतिवृत्तात्मक प्रश्नों की अपेक्षा नये तरीके से पूछ जाएँ जो उत्तर देने वाले को भी उत्तर के लिए प्रेरित करें। कई बार एक विषय पर अनेक लोगों के साक्षात्कार भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। तब प्रश्नमाला तैयार कर उनको भेजी जाए अथवा उनसे उत्तर माँगे जाए। उसके लिए एक सुन्दर विषय और आकर्षक शीर्षक होना आवश्यक है। प्रश्नकर्ता को सकारात्मक रूख अपनाना चाहिए। साक्षात्कार के लिए निर्धारित समय से पहले पहुँचना चाहिए। बहुत से लोग अपनी बात रिकार्ड नहीं करवाना चाहते। अथवा स्वयं को 'कोट' न करने का आग्रह करते हैं- लिखते समय इन बातों का सम्मान करना आवश्यक है। साक्षात्कार ऐसे वातावरण में समाप्त हो कि भविष्य में दुबारा मुलाकात में कठिनाई न हो।
फीचर लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुये उसके स्वरूप एवं महत्व का वर्णन कीजिये।
फीचर का अर्थ- 'फीचर' को अंग्रेजी शब्द Feature (फीचर) कां पर्याय कहा जाता है। फीचर शब्द को हिंदी में "रूपक" कहा जाता है। लेकिन आम भाषा में फीचर को ज्यादातर लोग फीचर ही कहते हैं। फीचर का अर्थ होता है- "किसी प्रकरण संबंधी (Sec- tional) विषय पर प्रकाशित आलेख है। लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित एक महत्वपूर्ण लेख की तरह एक महत्वपूर्ण लेख नहीं है।"
फीचर की परिभाषा - फीचर की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैंः
डी. एस. मेहता के अनुसार- "रोचक विषयों की विस्तृत व मनोरम प्रस्तुति ही
फीचर है। इसका उद्देश्य सूचना देना, मनोरंजन करना व जनता को जागरूक बनाना है। फीचर का अंतिम लक्ष्य ट्रेनिंग, मार्गदर्शन करना है।" डॉ. अर्जुन तिवारी के अनुसार - "मानवीय रुचि के विषयों के साथ सीमित
समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है तो वह फीचर की संज्ञा ले लेता है।"
फीचर के प्रकार - फीचर के प्रकार निम्नलिखित हैं:
1. व्यक्तिगत फीचर इसमें साहित्य, संगीत, चित्रकला, नाटकीय खेल जगत, राजनीतिक, विज्ञान, धर्म आदि क्षेत्रों में समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों- विशिष्ट व्यक्तियों पर फीचर लिखे जाते हैं।
2. समाचार फीचर - ऐसे फीचर का मूलभाव समाचार होते हैं। किसी घटना का पूर्ण विवेचन विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है।
3. त्यौहार पर्व संबंधी फीचर- विभिन्न पर्वों और त्यौहारों के अवसर पर इस तरह के फीचर लिखने का प्रचलन है। इसमें त्यौहारों पर्वों की मूल संवेदना उनके स्रोतों तथा पौराणिक संदर्भों के उल्लेख के साथ-साथ उन्हें आधुनिक संदर्भों में भी व्याख्यायित किया जाता है।
4. रेडियो फीचर- जहां पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित फीचर केवल पढ़ने के लिए होते हैं वहां रेडियो फीचर केवल प्रसारण माध्यमों से सुनने के लिए होते हैं इनमें संगीत और ध्वनि पक्ष काफी प्रबल होता है। रेडियो फीचर संगीत और ध्वनि के माध्यम से किसी गतिविधि का नाटकीय प्रस्तुतीकरण है।
5. विज्ञान फीचर - नवीनतम वैज्ञानिक उपलब्धियों से पाठकों को परिचित कराने अथवा विज्ञान के ध्वंसकारी प्रभावों की जानकारी देने का यह एक सशक्त और महत्वपूर्ण मध्यम है।
6. चित्रात्मक फीचर- ऐसे फीचर जो केवल बोलते चित्रों के माध्यम से अपना- संदेश पाठकों को दे जाते हैं। इसे फोटो फीचर कहते हैं।
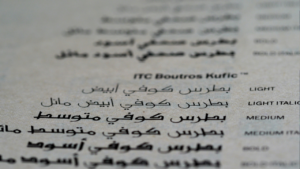
7. व्यंग्य फीचर - सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य की ताजा घटनाओं पर व्यंग्य करते हुए सरस और चुटीली भाषा में हास्य का पुट देकर लिखे गए फीचर इस कोटी में आते हैं।
8. यात्रा फीचर - यात्राएं ज्ञानवर्धक और मनोरंजक साथ साथ होते हैं। इन • यात्राओं का प्रभावपूर्ण एवं मनोहारी संस्मरणात्मक चित्रण इन फीचरों में होता है।
9. ऐतिहासिक फीचर- अतीत की घटनाओं के प्रति मनुष्य की उत्सुकता स्वाभाविक है। ऐतिहासिक व्यक्तियों, घटनाओं और स्मारकों अथवा नई एतिहासिक खोजों पर ( भी भावपूर्ण ऐतिहासिक फीचर लिखे जा सकते हैं।
फीचर से सम्बन्धित प्रमुख बातें- मोटे तौर पर फीचर लेखन के लिए 5 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है-
(1) तत्थ्यों का संग्रह- जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना है उससे जुड़े, तत्थ्यों को एकत्रित करना सबसे जरूरी काम है। तत्थ्यों और जानकारी को जुटाए बिना फीचर की रचना हो ही नहीं सकती। जितनी अधिक जानकारी होगी, फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। तत्थ्यों के संग्रह में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि तत्थ्य मूल स्त्रोत से जुटाए जाएं और वह एकदम सही हों। गलत तत्थ्यों से फीचर का प्रभाव ही उलटा हो जाता है।
(2) फीचर का उद्देश्य: फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु फीचर के उद्देश्य का निर्धारण है। किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता। किसी दुर्घटना से जुड़ा फीचर लिखने के लिए यह तय करना जरूरी है कि दुर्घटना के किस पहलू पर फीचर लिखा जाना है, दुर्घटना के इतिहास पर, दुर्घटना के प्रभावों पर, दुर्घटना की रोकथाम के तरीकों पर या दुर्घटना के यांत्रिक पक्ष पर। एक बार उद्देश्य तय हो जाए तो फीचर लेखन का चौथाई काम पूरा हो जाता है।
(3) प्रस्तुतिकरण : फीचर लेखन का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष है। फीचर लेखन में इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मनोरंजक हो। उसे सरस और सुबोध ढंग से प्रस्तुत किया जाए। तत्थ्यों का प्रस्तुतिकरण सहज हो और तत्थ्यों की अधिकता से पठनीयता खत्म न हो।
(4) शीर्षक तथा आमुख: किसी अच्छे समाचार की तरह ही अच्छे फीचर का शीर्षक और आमुख भी उपयुक्त ढंग से लिखा जाना चाहिए। अच्छे शीर्षक से पाठक सहज रूप से फीचर की ओर आकर्षित हो सकता है। खराब शीर्षक के कारण यह भी हो सकता है कि पाठक का ध्यान उसकी ओर जाए ही नहीं। इसी तरह अच्छा आमुख भी पाठक को बांध सकता है। बेतरतीब ढंग से लिखे आमुख के कारण पाठक में अरूचि पैदा हो सकती है। शीर्षक की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह पाठक को आकृष्ट भी कर ले, पाठक में विषय के प्रति जिज्ञासा भी पैदा करे और सार्थक भी हो। शीर्षक में सिर्फ शब्दों की तुकबन्दी या शब्दों के ध्वन्यात्मक प्रभावों की अधिकता के प्रयोग से भी बचा जाना चाहिए।
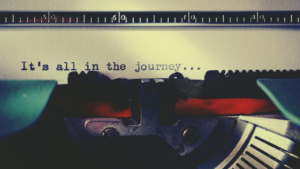
(5) साज सज्जा : लेखन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी पर्याप्त साज संज्जा की तैयारी पूरी न हो जाए। फीचर के साथ इस्तेमाल होने वाले चित्रों, रेखाचित्रों और
ग्राफिक्स का चयन भी फीचर रचना का एक जरूरी पहलू है। छपाई की वर्तमान तकनीक के कारण फीचर की साज सज्जा अब बेहद आसान हो गई है और उसमें तरह-तरह के प्रयोग करने की गुजांइश भी बढ़ गई है।
फीचर लेखन एक कला भी है और अब जबकि फीचर का स्वरूप बदल रहा है तो फीचर लेखन की तकनीक और तरीके भी बदल रहे हैं। वर्तमान में फीचर अपनी परम्परागत शैलियों और परिभाषाओं की सीमा तोड़ कर नए-नए रूप बदलते जा रहे हैं।

Post a Comment